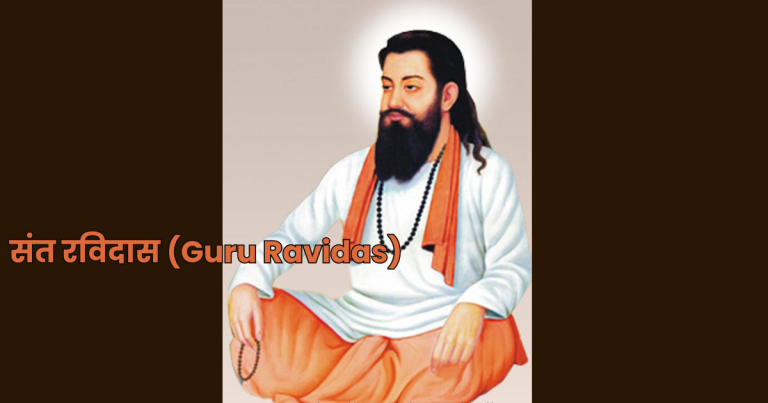
पंद्रहवीं शताब्दी को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यह काल भारत में संतों के द्वारा चलाए गए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आंदोलन का काल है। इस काल में एक नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है और वे है संत रविदास (Ravidas) जी। संत रविदास (Ravidas) को हम अक्सर भक्ति कवि, निर्गुण संत और जातिवादी बंधनों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले संत के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर परिवर्तनवादी दृष्टिकोण (यानी सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन, संरचनात्मक असमानताओं के विरोध और वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण के नज़रिए) से देखें, तो उनका जीवन और विचार कहीं ज़्यादा गहरे और क्रांतिकारी दिखाई देते हैं।
प्रारंभिक जीवन: संत रविदास (Ravidas) जी का जन्म लगभग 1450 ईस्वी के आसपास वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के पास सीर गोवर्धनपुर गाँव में हुआ माना जाता है। वे चर्मकार (मौची जाति) समुदाय से थे, जो उस समय अछूत और नीची जाति मानी जाती थी। उनके पिता का नाम संतोक दास और माता का नाम कलबो देवी (करमा देवी) बताया जाता है। परिवार का पारंपरिक व्यवसाय चमड़े का काम था।
बचपन और शिक्षा: बचपन से ही रविदास (Ravidas) जी का मन ईश्वर भक्ति, सेवा और समानता की ओर झुका हुआ था। वे गुरुकुल या ब्राह्मण पंडितों की औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे, क्योंकि जाति-व्यवस्था ने नीची जातियों के लिए यह रास्ता बंद कर रखा था। जाति की वजह से समाज ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन रविदास (Ravidas) जी ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि ईश्वर के सामने सब समान हैं।
पारिवारिक जीवन: संत रविदास (Ravidas) जी को अक्सर उनकी भक्ति और सामाजिक क्रांति के संदर्भ में ही याद किया जाता है, लेकिन उनका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कभी सांसारिक जिम्मेदारियों से पलायन नहीं किया।
संत रविदास (Ravidas) जी का विवाह लोना देवी नामक महिला से हुआ था। लोना देवी भी चर्मकार समुदाय से थीं। उनका विवाह इस बात का प्रमाण है कि रविदास (Ravidas) जी ने गृहस्थ जीवन अपनाया और संत बनने के लिए संन्यास या पलायन का रास्ता नहीं चुना। संत रविदास (Ravidas) जी की संतान के बारे में अलग-अलग परंपराओं में अलग जानकारी मिलती है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि उनकी एक पुत्री मानी जाती है, जिसका नाम कुमारी करुणा था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्होंने कोई संतान नहीं छोड़ी, और उनके शिष्यों व अनुयायियों को ही उन्होंने अपना परिवार माना। रविदास (Ravidas) जी ने विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने व्यवसाय और भक्ति-साधना को संतुलित रखा। उनकी पत्नी लोना देवी उनके कार्य में सहयोग करती थी।
उस समय बहुत-से संत (जैसे कबीर, दादू, नामदेव) भी गृहस्थ जीवन जीते थे, ताकि यह सिद्ध हो कि साधना के लिए गृह-त्याग अनिवार्य नहीं। रविदास (Ravidas) जी ने भी यही दिखाया कि गृहस्थ, श्रमजीवी और समाज के बीच रहते हुए भी संत और समाज-सुधारक बना जा सकता हं। यह उनके विचारों का व्यावहारिक उदाहरण है कि सच्चा संत वही है, जो समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी न्याय और भक्ति का मार्ग दिखाया।
इसके बावजूद उन्होंने लोकभाषा (खड़ीबोली, ब्रज, अवधी मिश्रण) में ज्ञान अर्जित किया और वही उनकी रचनाओं की भाषा बनी।
समानता और जाति-उत्पीड़न का प्रतिरोध:
उन्होंने साफ़ कहा कि ईश्वर के दरबार में ऊँच-नीच नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन वे केवल आध्यात्मिक समानता की बात तक सीमित नहीं रहे। उनके पदों में सामाजिक बराबरी की व्यावहारिक आकांक्षा दिखती है, जैसे – “ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट-बड़ो सब सम बसे, रैदास रहै प्रसन्न॥” यह उनके समानता आधारित वैकल्पिक राज्य का स्वप्न है, जो परिवर्तनवादी सोच का एक अनछुआ पहलू है।
ब्रह्मांडीय भक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति:
रविदास (Ravidas) जी की भक्ति सामाजिक मुक्ति का साधन थी। उनका ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या वेद तक सीमित नहीं, बल्कि सबमें व्याप्त था। यह दृष्टिकोण धार्मिक सत्ता की केंद्रीकरण व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने ब्राह्मणों की धार्मिक ठेकेदारी के खिलाफ आवाज उठाई।
निर्भीकता और संवादशीलता:
वे कभी भी उच्च वर्णों के शास्त्रगत तर्कों से डरते नहीं थे। उनके समकालीन कबीर(Kabir), मीराबाई (Mirabai) और कई राजवंशी भी उनसे संवाद करते थे। उन्होंने निर्भीक होकर कहा – “जाति-जाति में जाति हैं, जो केलन के पात। रैदास मनुष न जुड़ सके, जब तक जाति न जात॥” यह सिर्फ़ जाति की आलोचना नहीं, बल्कि जाति-व्यवस्था की संपूर्ण अस्वीकृति है।
संसाधनों के समान बंटवारे की दृष्टि:
उनकी रचनाओं में ‘सबको अन्न मिले’ और ‘प्रकृति के सभी संसाधनों पर सबका अधिकार’ जैसी बातें झलकती हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण:
वे श्रम, उत्पादन और वितरण की बराबरी पर ज़ोर देते हैं—ये बातें आज के समाजवादी या परिवर्तनवादी चिंतन से जुड़ती हैं।
वैश्विक दृष्टि:
उनके विचार केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि “मानव” की एकता पर टिके हैं। यह उस समय की सामंती सीमाओं को तोड़ने वाला नजरिया था।
राज्य का वैकल्पिक मॉडल:
उनका “बेगमपुरा” (Begampura) सिर्फ़ आध्यात्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज का राजनीतिक घोषणापत्र है।
साहित्यिक योगदान:
संत रविदास (Ravidas) जी का साहित्य न सिर्फ़ भक्ति-आधारित है, बल्कि उसमें समानता, सामाजिक न्याय, श्रम की महिमा और जातिव्यवस्था के विरोध की स्पष्ट आवाज़ मिलती है। इसे हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं — रचनात्मक पक्ष और विचारधारात्मक पक्ष।
संत रविदास (Ravidas) जी निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से पद के रूप में हैं, जो लोकभाषा (खड़ीबोली, ब्रज और अवधी मिश्रण) में लिखे गए। उन्होंने शुद्ध संस्कृत या फारसी के बजाय जनभाषा का प्रयोग किया, ताकि हर वर्ग तक संदेश पहुँच सके।
उनकी रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब (Granth Sahib) (सिख धर्मग्रंथ) में शामिल हैं। इसमें संत रविदास (Ravidas) जी के लगभग 41 पद संग्रहीत हैं। उनके पद ‘संत साहित्य’ और ‘निर्गुण भक्ति काव्य’ के अंतर्गत अलग-अलग संकलनों में भी मिलते हैं। लोक-परंपरा में उनकी वाणी को रविदासिया पंथ के अनुयायी आज भी गाते और संजोते हैं।
साहित्यिक शैली:
उनकी शैली भाषा सरल, सीधी और भावपूर्ण थी। उसमें वे उदाहरण, उपमा और रूपकों का सहज प्रयोग करतें। वे उच्च कोटि के साहित्यिक थे तथा उनका साहित्य अलंकरणों के बजाय जन-संवाद शैली में था।
प्रभाव:
उनकी वाणी ने बहुजन और श्रमिक समाज को आत्मगौरव और समानता का संदेश दिया। गुरु नानक और सिख परंपरा पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आधुनिक बहुजन साहित्य और चिंतन की जड़ें संत रविदास (Ravidas) की वाणी में दिखाई देती हैं।
परिवर्तनवादी नज़रिए से संत रविदास (Ravidas) जी का जीवन एक श्रम-आधारित समाज, जाति-मुक्त समानतावादी व्यवस्था और वैकल्पिक न्यायपूर्ण राज्य की कल्पना है। वे केवल संत नहीं थे, बल्कि अपने समय के सामाजिक क्रांतिकारी भी थे, जिनकी आवाज़ आज भी परिवर्तन की प्रेरणा देती है।
