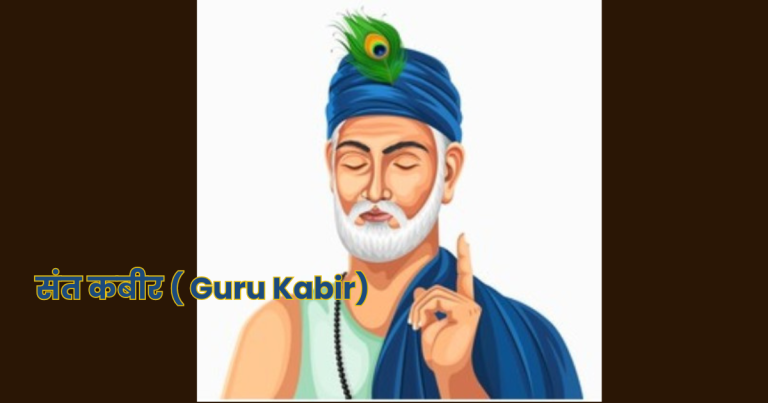
भारत मे संतों के आंदोलन को ‘भक्ति आंदोलन ‘(Bhakti Andolan) के नाम से जाना जाता है। सातवीं सदी में दक्षिण से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन (Bhakti Andolan) १३ वी सदी में मध्य भारत से होता हुआ १५ वी से १७ वी सदी तक उत्तर भारत में पहुंच कर राष्ट्रव्यापि बन गया। १५ वी से १७ वी सदी में सुफि और भक्ति आंदोलन (Bhakti Andolan) अपने चरम पर था। इस समय भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। इसी काल में भारतीय संतों की कड़ी में संत कबीर (Kabir) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनका जीवन और कार्य भक्ति आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
परिचय: संत कबीर (Kabir) का जन्म 15 वी शताब्दी (लगभग 1440) में भारत के वाराणसी शहर में लहरतारा गांव में हुआ। वे एक बुनकर (जुलाहा) मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और अपने जीवन के दौरान सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में पहचाने गए। उनके जन्म सम्बन्धी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि वे नीरू और नीमा नामक जुलाहा दम्पत्ति के पुत्र थे, जबकि कुछ मानते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दे कर नदी किनारे छोड़ दिया। निमा और निरु नामक जुलाहा (मुस्लिम) दंपति ने उनका पालनपोषण किया।
कबीर का जीवन और उनकी शिक्षा एक ऐसे समय में आयी जब भारत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। कबीर (Kabir) ने हिन्दू और मुस्लिम दोनों में व्याप्त जातिप्रथा, कर्मकांड, पाखंड का कडा विरोध किया और ममता, प्रेम और समता पर जोर दिया। उन्होंने अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से लोगों को नैतिक और सामाजिक संदेश दिया, जो आज भी प्रासिंगिक है।
जीवनयापन: कबीर (Kabir) जुलाहे (बुनकर) का काम करते थे। वे साधारण जीवन जीते थे और श्रम को ही सर्वोपरि मानते थे।
धार्मिक पृष्ठभूमि: वे न तो पूर्ण रूप से हिन्दू परंपरा में बंधे थे और न ही मुस्लिम मतों के अनुयायी। उन्होंने दोनों धर्मों की रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना की।
सामाजिक समता: कबीर (Kabir) ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव का विरोध किया और समता पर बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सभी मनुष्यों को समान दृष्टि
से देखने की शिक्षा दी।
नैतिक शिक्षाएं: कबीर (Kabir) के दोहे और साखियां नैतिकता और जीवन के उच्च आदर्शों की शिक्षा देती है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, और सच्चाई की शिक्षा दी और लोगों को अपने आचरण में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
संत कबीर का कार्य और योगदान
1. धार्मिक दृष्टिकोण: संत कबीर (Kabir) को भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तम्भ माना जाता है। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया।
“मोको कहां ढूंढे रे बन्दे
मैं तो तेरे पास में..!
इस पुरे भजन के माध्यम से कबीर ने उनका धार्मिक दृष्टिकोण साफ़ साफ़ नज़र आता है। कबीर (Kabir) कहते थे कि ईश्वर निराकार है, उसे मंदिर–मस्जिद में ढूँढना व्यर्थ है। उन्होंने “सत्य नाम” को ही परमात्मा का स्वरूप बताया।
2. समाज सुधार: उन्होंने जाति-पाँति, ऊँच-नीच, और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। कर्मकांड, मूर्तिपूजा, बाहरी दिखावे, और धार्मिक कट्टरता की आलोचना की और मानवता, प्रेम और समानता पर बल दिया।
3 लैंगिक समानता और सशक्तिकरण: संत कबीर (Kabir) का लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण उनके समय से कई आगे था। उन्होने अपने समय में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों और अन्याय का विरोध किया। कबीर (Kabir) ने अपनी कविताओं और दोहों में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और
उन्हे समान अधिकार देने पर जोर दिया। कबीर का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से ईश्वर की रचना और इसलिए दोनों के बीच भेदभाव अनुचित है। उन्होंने
महिलाओं को भी आध्यात्मिक साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
“नारी नरक न जाने कोई, जाने वो नारी अपमान।
नारी नरक का मूल नहीं, देखो संत कबीर बखान।।”
इस दोहे में कबीर (Kabir) महिलाओं के प्रति होने वाले अपमान और भेदभाव का कडा विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाएं नरक का कारण नहीं है, बल्कि उनके प्रति
अन्याय और अपमान नरक का मूल है। कबीर (Kabir) ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार है। उन्होने महिलाओं को सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में समान अधिकार देने की वकालत की।
4. कबीर (Kabir) की वाणी: उनकी रचनाएँ “साखी”, “सबद” और “रमैनी” के रूप में प्रचलित हैं। बाद में उनकी वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित की गई। उनकी भाषा शैली सरल, सहज और लोकजीवन से जुड़ी हुई रही—जिसे “सधुक्कड़ी” कहा जाता है।
5. कबीर (Kabir) का सामाजिक साहस: संत कबीर का जीवन समाज को अंधविश्वास और भेदभाव से मुक्त करने का एक महान प्रयास था। कबीर केवल धार्मिक रूढ़ियों पर ही प्रहार नहीं करते थे, बल्कि राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था की कमजोरियों पर भी टिप्पणी करते थे।
कंकर पाथर जोर के, मस्जिद ली बनाए।
था चढि मुल्ला बांक दें, क्या बहरा हुआ खुदाय।।
जो तूं ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया।
आन बांट काहे नहीं आया।।
मुरख लोग जानी न लिन्हि, पुराननि की बातें।
कबीर क़साई क़साई है, नहीं राम सौ लाते।।
उन्होंने पंडित, मुल्ला, धनी और शासकों तक को चुनौती दी। उनके लिए सच्चा धर्म किसी भी सत्ता या वर्ग के सामने झुकना नहीं बल्कि सत्य बोलना था।
6. प्रभाव: कबीर (Kabir) की वाणी ने हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदायों को प्रभावित किया। उनके विचारों ने सिख धर्म पर भी गहरा असर डाला। आज भी उनकी वाणी लोगों को सत्य, सरलता और मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। संत कबीर जातिप्रथा, छुआ-छूत और कर्मकांड पर प्रहार करनेवाले महान कवि और क्रांतिकारी समाज-सुधारक थे।
7. श्रम और साधना का संगम: कबीर केवल उपदेशक ही नहीं थे, बल्कि कर्मयोगी थे। वे जीवन भर बुनकर का काम करते रहे और सच्चा भक्ति मार्ग वही है जो रोज़ी-रोटी कमाने के श्रम के साथ जुड़ा हो। इस दृष्टि से वे भारतीय परंपरा में काम और ध्यान को साथ रखने वाले संत माने जाते हैं।
मृत्यु:
कबीर (Kabir) का अंतिम समय मगहर में बीता। मान्यता थी कि वहाँ मरने से नरक मिलता है, जबकि काशी में मरने से मोक्ष। कबीर ने इस मान्यता को तोड़ने के लिए काशी नहीं बल्कि मगहर में देहत्याग किया। लेकिन उनकी मृत्यु भी रहस्य से भरी है। उनकी मृत्यु के समय हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में विवाद हुआ कि अंतिम संस्कार कैसे हो। कहा जाता है कि जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तो वहाँ फूलों का ढेर मिला। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति मरे और उसका शव विलुप्त हो जाए।
समाज में ऐसा मत भी प्रचलित है कि उस समय राजनीतिक तथा धार्मिक ठेकेदारो की चूले हिल गई थी। क्योंकि समाज में हिन्दू और मुस्लिमों में उनके अनुयायियों की भरमार हो गई थी। जो विषमता तथा सत्ता परिवर्तन का द्योतक बन सकती थी। इसलिए ब्राह्मणवाद का दांव खेला गया और उनकी मृत्यु को चमत्कार बनाने का ड्रामा खेला गया।
जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहां शव के बजाय फुलों का ढेर मिला। हिंदुओं ने आधे फूल जलाकर चिता दी और मुसलमानों ने आधे फूल दफनाए।
इन अनछुए पहलुओं से स्पष्ट होता है कि कबीर केवल संत या कवि नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और निर्भीक विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सत्य और मानवता धर्म से भी ऊपर है। शायद इसीलिए आधुनिक भारत के महानायक बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर (Dr Bhimrao Ambedkar) ने उनको अपना गुरु माना। आज भी भारत का मानवतावादी आंदोलन उनके संदेश को याद किए बगैर चलाया नहीं जा सकता।
