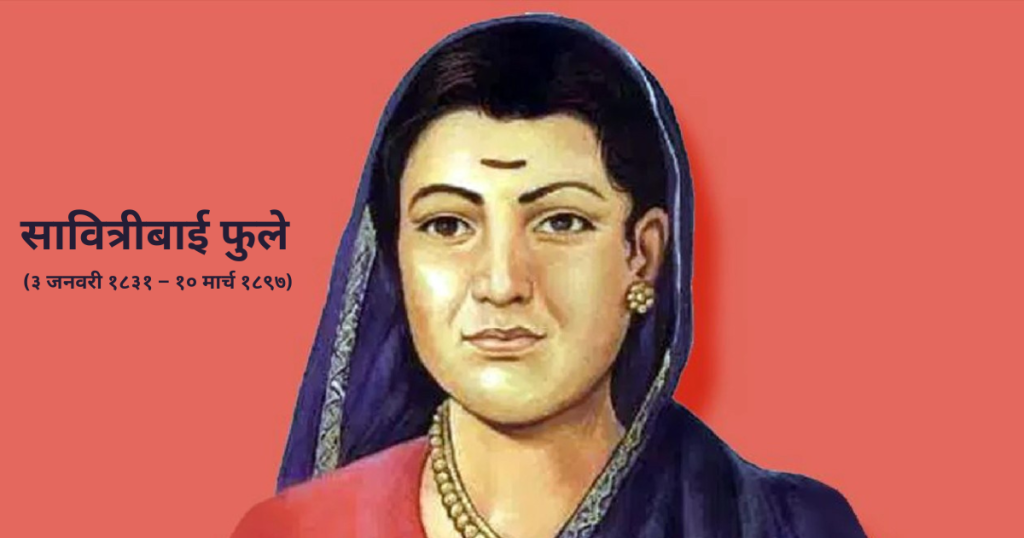
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule): एक अतुलनीय व्यक्तित्व
(३ जनवरी १८३१ – १० मार्च १८९७)
सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले (Savitribai Phule) का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के नायगाँव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) का बचपन बहुत सादगीपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम खंदोजी नवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय समाज में लड़कियों को पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं थी। रूढ़िवादी परंपराओं के कारण उनका बचपन शिक्षा से वंचित रहा। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह 12 वर्षीय ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) से कर दिया गया। उस समय बाल विवाह की प्रथा आम था।
विवाह के बाद उनके पति ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाया। धीरे-धीरे सावित्रीबाई पढ़ाई में निपुण हो गईं और आगे चलकर उन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) के साथ मिलकर वंचितों और पिछड़े वर्गों के बच्चों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) का परिवार भी महिला शिक्षा के पक्ष में नहीं था। लेकिन ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) की जिद्द के फलस्वरूप ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) और उनकी जिवन संगिनी को शिक्षा प्रदान करने के कार्य से उनका परिवार रोक नहीं पाया। शिक्षा प्रसार के विरोध में समाज के दबाव फलस्वरूप ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) के पिता जी ने उन्हें शिक्षण कार्य को बंद करने के शख्त निर्देश दिए लेकिन सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने घर से बाहर जाना स्वीकार किया । घर से निकलने के बाद उन्होंने फ़ातिमा शेख (Fatima Sheikh) और उनके भाई उस्मान शेख (Usman Sheikh) के घर में रह कर शिक्षण कार्य किया। शिक्षा के कार्य मे सावित्री बाई (Savitribai Phule) को फ़ातिमा का भरपूर सहयोग मिला। सावित्री बाई (Savitribai Phule) और फ़ातिमा शेख (Fatima Sheikh) ‘टीम’ के रूप में शिक्षण कार्य किया । उन्होंने फ़ातिमा शेख़ (Fatima Sheikh) के साथ मिलकर गंजपेठ (पुणे) में भी दूसरा स्कूल चलाया। फ़ातिमा शेख़ (Fatima Sheikh) केवल सह-शिक्षिका नहीं थीं, वे अपने घर में कक्षाएँ चलवाकर सामाजिक प्रतिरोध के बीच सुरक्षा-वातावरण भी बनाती थीं। सावित्री बाई की लगन और ज्योतिराव फुले का सहयोग उन्हें समाज सुधारक और भारत की पहली महिला शिक्षिका होने के गौरवपूर्ण मकाम तक लेकर गया।
आगे चलकर उन्होंने शिक्षा में ट्रेन्ड टिंचर की विशेष योग्यता प्राप्त की और व्यापक रूप से समाजसेवा के मार्ग पर अग्रसर हुईं।
अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में हुए अपमान ने ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार तथा व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में खड़ा का संकल्प लिया था जिसे उन्होंने जीजान लगाकर अत्यंत गतिरिधों एवं संघर्षों के पश्चात पूर्ण किया । स्वर्ण समाज तथा अपने समाज के घोर विरोध के बावजूद फुले दम्पत्ति ने अध्यापन कार्य को लगातार जारी रखा।
सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) के साथ मिलकर भिड़े वाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule के देहांत के बाद भी शिक्षण कार्य जारी रखा जिसे वे मरते दम तक करती रही।
सावित्रीबाई मिशनरी शिक्षिकाओं और स्थानीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर ‘शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग’ करवाती थीं। समकालीन विवरण बताते हैं कि उन्होंने “नॉर्मल” कक्षाओं से सीखकर प्रशिक्षण की विधियों को अपने पाठ्यक्रम में भी अपनाया।
कक्षा के भीतर उनकी अध्यापन-दृष्टि और तौर-तरीके बहुत ही सराहनीय थे। वे पढ़ना-लिखना और गणित तो सिखाती ही थीं, उसके साथ-साथ स्वच्छता, शिष्टाचार, नागरिक विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान (घरेलू लेखा, चिट्ठी लिखना) पर खास ज़ोर देती थीं; ताकि शिक्षा सीधे समाज के जीवन-परिवर्तन लाये और उनकी जीवन चर्या आसान हो।
उन्हें कविता लिखने का भी बडा शौक था। उनका कविता संग्रह “काव्यफुले” के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कविताए न केवल साहित्य बल्कि उनमें समाज के लिए पर्याप्त प्रेरणा भी मौजूद थी। उनकी कविताए छात्राओं में आत्मविश्वास, जाति भेद व लिंग भेद आधारित हीनभावना के प्रतिरोध और शिक्षा के मानव जीवन खासकर महिलाओं जीवन मे महत्व को दृढ़ करती थीं। तत्कालीन सामाजिक स्थिति को जानकर किस प्रकार की कविताएं पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगी इसका वे बहुत बारीकी से ध्यान रखती और वैसी ही कविताओं की रचना कर पाठ्यक्रम में शामिल करती।
वे लड़कियों की “स्कूल आने” की उम्मीद भर नहीं रखती थीं। बल्कि उनके घरों तक जाकर परिजनों को मनाना, विरोध झेलते हुए भी छात्राओं को नियमित बनाए रखना उनकी दिनचर्या थी। जब कुछ ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक लोगों द्वारा उनपर और फ़ातिमा के ऊपर पत्थर/गोबर फेंके जाने की घटनाएँ शुरू हुई तो वे एक अतिरिक्त साड़ी साथ रखतीं और साड़ी पर गोबर/किचड़ फेंके जाने पर उसे बदलकर फिर पढ़ाने लगतीं।
अध्यापन के इस कार्य को वे बड़े ही आधुनिक तरीके से करती। बच्चों की शिक्षा का डेटा संकलन तथा स्कूल में कठोर अनुशासन उनके कार्य की विशेषता थी। तदकालीन रिपोर्टों में लड़कियों की उपस्थिति-पंजिका प्रगति-अभिलेख और मासिक आकलन सभी अंकित मिलते हैं। यानि वे भावनात्मक अपील के साथ ही व्यवस्थित शैक्षिक प्रबंधन भी करती थीं।
ज्योतिबा फुले (Jyotiba Phule) तथा सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) के अथक प्रयासों से जगह-जगह इतने स्कूल खुल गये थे कि उसने एक संस्था का रुप ही ग्रहण कर लिया था। बड़े क्षेत्र में वंचितों और शोषितो के लिए स्कूलों का बहुत विकास किया गया। 1848–50 के बीच पुणे में कई बालिकाओं के स्कूल खुले। बाद के वर्षों में तमाम पिछड़े जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अलग-अलग बस्तियों में केंद्र स्थापित किए गए। जिससे स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद पहुँच बनी रहे।
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) ने स्त्रियों की बैठकों का एक मंच/मंडल खड़ा किया, जहाँ विधवा उत्थान-कुप्रथा उन्मूलन, प्रसूति उपचार तथा प्रसव कराने हेतु स्वच्छ वातावरण के साथ साथ चिकित्सीय सुविधा स्वास्थ्य, संपत्ति-अधिकार, विधवा-पुनर्विवाह जैसे विषयों पर लोकभाषा में भाषण और संवाद सुसंवाद कराये जाते थे।
फुले दंपती ने अपने कुएँ को सभी जातियों के लिए खोल दिया। यह प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि जिन्हें पानी नहीं दिया जाता उनके लिए दैनिक पानी की पहुँच से जुड़ा जीवंत सामाजिक हस्तक्षेप था।
उन्होंने स्त्री-अधिकार की व्याख्या की तथा महिलाओं के लिए “सुरक्षा-जाल” बनाया। वर्ष 1860 में अवांछित/असुरक्षित गर्भ—खासकर विधवाओं के लिए बालहत्या प्रतिबंधक गृह बनायें। बालहत्या रोकने और माँ-शिशु की देखभाल हेतु आश्रय-गृह चलाया। वहाँ प्रसव-सहायता, पोषण, पुनर्वास और शिक्षा-सलाह दी जाती थी। यह अपने समय का समग्र सामाजिक-कार्य का आधुनिक मॉडल था।
अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रथा की शुरुआत फुले दंपती ने की। एक ब्राह्मण विधवा द्वारा परित्यक्त शिशु यशवंतराव को फुले दंपती ने गोद लिया; जो आगे चलकर चिकित्सक बने और प्लेग-राहत में माँ सावित्री बाई के साथ काम किया। यह बताता है कि उनका विमर्श केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन था।
उस समय ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह- कल्पना से परे था। लेकिन फुले दंपती ने (Self-Respect/Satyashodhak Marriage) सत्य शोधक विवाह पद्धति का आविष्कार किया। उन्होंने ऐसे विवाह आयोजित कराए जिनमें ब्राह्मण पुरोहित, दहेज, और शास्त्रोक्त कर्मकांड अनिवार्य नहीं थे। सगाई/विवाह को समानता-आधारित अनुबंध और प्रतिज्ञाओं की रचना कर आधार दिया।
सार्वजनिक विरोध से निपटने के लिए उन्होंने एक रणनीति के साथ कार्य किया। उन्होंने मुस्लिम पड़ोसियों सहित विविध समुदायों के साथ काम किया। जैसे, रहने के लिए तथा स्कूल के लिए सुरक्षित स्थान मिलना ( शेख़ उस्मान परिवार का घर) और पहलवान लहुजी साल्वे की पुरी टिम ने सामुदायिक पहरेदारी की जिम्मेदारी उठाना।
अपने शिक्षा अभियान को और मजबूती तथा विस्तार देने के लिए उन्होंने अधिकारिक मान्यता का उपयोग बहुत अच्छे से किया। जब शिक्षा बोर्ड अधिकारियों से प्रशंसा-पत्र या प्रोत्साहन मिलता, तो वे इन्हें लोकमत बदलने के लिए एक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल करतीं। कहती, “देखिए, हमारी लड़कियाँ सीख रही हैं और इसे सरकार भी मान रही है।”
सावित्रीबाई फुले के लेखन, भाषण और विचार-रेखा कृतियाँ बतौर आंदोलन की दस्तावेज़ बन गई है। “काव्यफुले” (1854) और “बावनकशी सुबोध रत्नाकर” (1892) में स्त्री-स्वाभिमान, जाति-विरोध, शिक्षा-न्याय के विचार मिलते हैं। वे भाषा को सरल रखतीं ताकि निम्न-पठनीय वर्ग तक बात पहुँचे।
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) ने विमर्श की एक धारा का ही शृजन किया था। उनका काम केवल “स्त्री-शिक्षा” तक सीमित नहीं; तो वह जाति-आधारित बहिष्कार का आलोचनात्मक खात्मा, आर्थिक-न्याय (श्रम, रोज़गार कौशल), और सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वच्छता/प्लेग-राहत) तक फैला था। आज की भाषा में कहें तो वे जेंडर, जाति और वर्ग के जोड़ पर सोचती और काम करती थीं।
महामारी की आपातकालीन स्थिति में सावित्रीबाई तथा उनकी पुरी टिम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा सेवा की सूक्ष्म तस्वीर (1897) प्रस्तुत करती है। पुणे में प्लेग के दौरान उन्होंने राहत-केंद्र/क्लिनिक गठित किया। रोगियों को घर से उठाकर उपचार तक पहुँचाने की उन्होंने व्यवस्था की। कहा जाता है कि एक बीमार बालक को स्वयं कंधों पर उठाकर ले जाते हुए वे संक्रमित हुईं। इसी से 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हुई। यह घटना यूँ ही नहीं बताई जाती। यह उनकी नैतिकता, मानवता तथा व्यक्तिगत जोखिम उठाकर भी सेवा देना उनके समर्पण की परिचायक है।
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) ने अपनी विरासत में समाज को स्कूल, महिला-मंडल, आश्रय-गृह, पानी/स्वास्थ्य जैसे बहु-क्षेत्रीय संस्थागत मॉडल ने आगे के सामाजिक आंदोलनों को “एकीकृत सेवा-संरचना” का रास्ता दिखाया।
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) सार्वजनिक मंचों पर स्त्री-आवाज़ बनी। वे सार्वजनिक मंचों पर बोलने वाली शुरुआती स्त्रियों में थीं। यानि स्त्रियों का “घर के भीतर” सीमित होना, उनके रहते मानदंड नहीं रहा। वे समकालीन प्रेरणा बनकर हमारे सामने है। आज की एनजीओ/कम्युनिटी-स्कूलिंग, डिप एन्ड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स, प्लानर, ऑर्गनाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेनर और निडरता के साथ बिना-पुरोहित/लो-कॉस्ट विवाह जैसे प्रचलनों में उनका बौद्धिक तथा साहसीक पदचिन्ह साफ़ दिखता है। सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) केवल “पहली शिक्षिका” नहीं, बल्कि शिक्षक-प्रशिक्षण से निकली पद्धतियों को लागू करने वाली ही नहीं तो समकालीन परिदृश्य में हर प्रकार के दमन उत्पीड़न, संकोच तथा निराशा बाहर निकालने कीब आधी आबादी के लिए प्रेरणा बन गई है।
